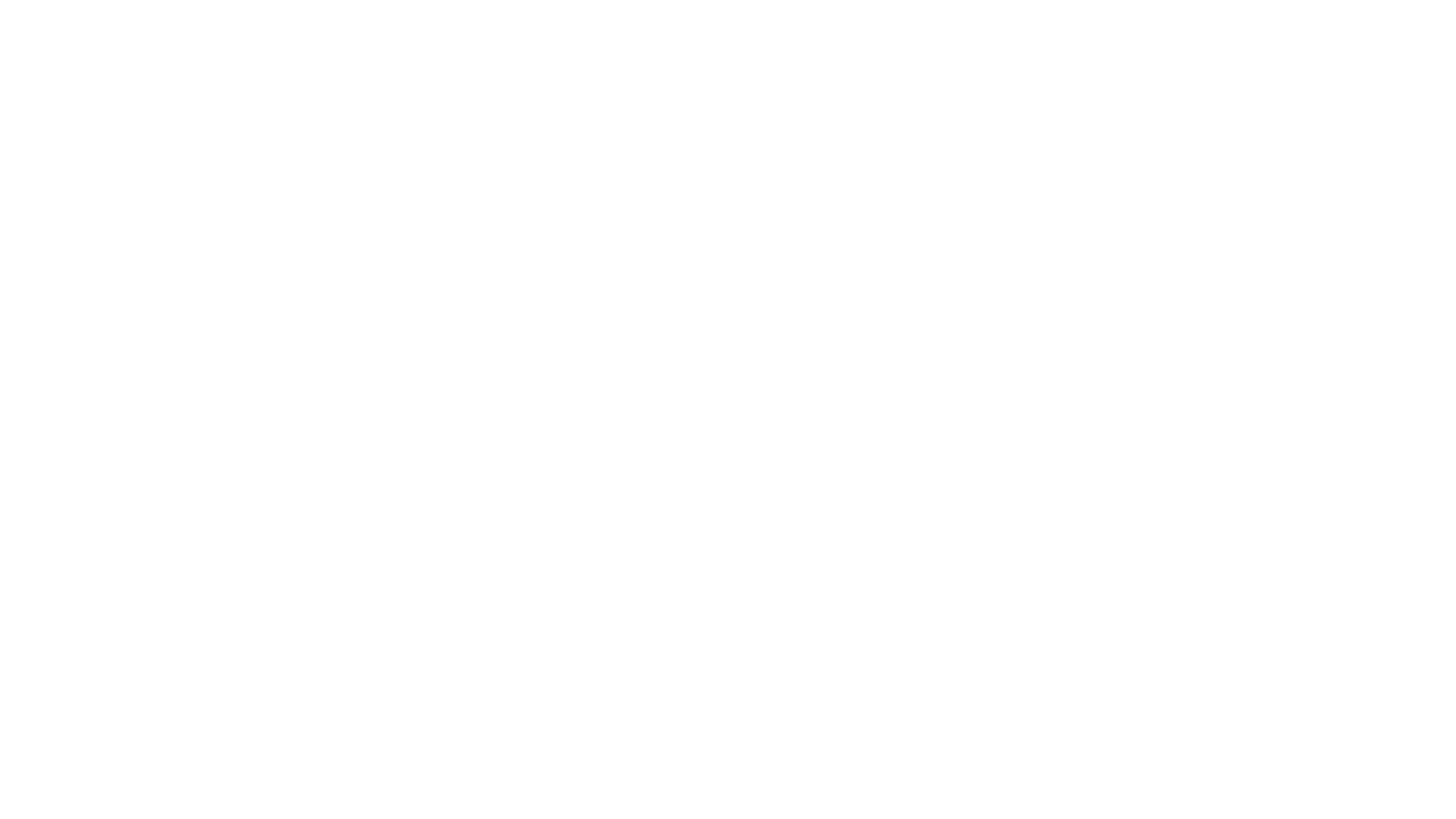-दीपक रंजन दास
बाल सुधार गृह बच्चों को अपराध से दूर करने में नाकाम सिद्ध हुए हैं. तमाम काउंसलिंग और अन्य कोशिशें भी बेअसर साबित हुई हैं. बाल सुधार गृह बच्चों का न तो नशा छुड़ा पा रहे हैं और न ही उनमें कानून का खौफ जगा पा रहे हैं. बाल सुधार गृह ही क्यों, केन्द्रीय कारागार भी अपराधियों में कानून का भय पैदा करने में नाकाम सिद्ध हुए हैं. उलटे ये संस्थान अपराध का प्रशिक्षण केन्द्र बन गए हैं. जब बालक या अपराधी इन संस्थानों से निकलता है तो वह पहले से ज्यादा निडर, पहले से ज्यादा खूंखार और संगठित होता है. सभ्य समाज बालिग और नाबालिग को परिभाषा में बांधता है. तमाम ऐसी बहसें होती हैं जिसमें अंत-पंत ऐसा लगने लगता है कि अपराधी-अपराधी नहीं है. सारा दोष परिवेश, परवरिश और परिस्थितियों का है. यदि यह सही है तो इसे बदलने की जरूरत है. आखिर क्या कुछ बदला है पिछले कुछ दशकों में? 80 के दशक का बच्चा शाम को मैदान में होता था. 2-3 घंटा खेलकर वह इतना थक चुका होता था कि घर में घुसते ही रोटी मांगता था. होमवर्क पूरा करने से पहले ही उसकी आंखें मुंद जाती थीं. सुबह एक पुकार पर उठ जाता था और स्कूल पहुंच जाता था. वहां भी पढ़ाई के साथ-साथ इतनी शारीरिक क्रियाएं होती थीं कि घर लौटते ही वह बस्ता फेंककर खाना मांगता था. बच्चे के हाथ पैर धुलाना तक मुश्किल हो जाता था. शिक्षक भी एक ही लाइन का मोटिवेशन देते थे – बेटा यह तुम्हारे खेलने, खाने और पढऩे के दिन हैं. ज्यादा टेंशन मत लो. धीरे-धीरे सबकुछ बदल गया. कुछ तो बढ़ती जरूरतें और कुछ सशक्तिकरण का नारा, दोनों ने मिलकर एकल परिवारों के बच्चों को अलग-थलग कर दिया. टीवी, मोबाइल और ओटीटी ने मनोरंजन को एक नई दिशा दे दी. खेल मैदानों से बच्चे गायब हो गए. पार्कों में सुबह अधेड़ों और बूढ़ों का डेरा हो गया. एकांत मनोरंजन की अपनी समस्याएं हैं. कोई नशे का ग्राहक बन जाता है तो कोई सौदागर. उसकी यौन इच्छाएं भड़कने लगती हैं. सरकार कहती है कि उसने पोर्न साइट्स बैन कर दिये हैं. हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है. खोजने वालों को सबकुछ मिल जाता है. यह मनुष्य की आदिम इच्छाओं में से एक है. कुंठा इसे विकृत कर देती है. ऐसा व्यक्ति सॉफ्ट टारगेट ढूंढता है. अबोध बच्चियां उनकी इसी जरूरत को पूरा करती हैं. बलात्कार के अधिकांश मामलों में इसीलिए अपराधी कोई करीबी रिश्तेदार या परिचित होता है. टीवी, मोबाइल, ओटीटी को बंद नहीं किया जा सकता पर बच्चों को व्यस्त किया जा सकता है. सभी बच्चों को शिक्षा के गन्नारस मशीन में पेरने की आवश्यकता नहीं है. यह सबके बस का रोग भी नहीं है. आंकड़ेबाजी को दरकिनार कर इस दिशा में शोध करना होगा. खाली दिमाग को शैतान का घर बताया गया है. सकारात्मक-रचनात्मक व्यस्तता ही इसका एक मात्र हल प्रतीत होता है.
गुस्ताखी माफ: हैवानियत की हदें और बाल सुधार गृह