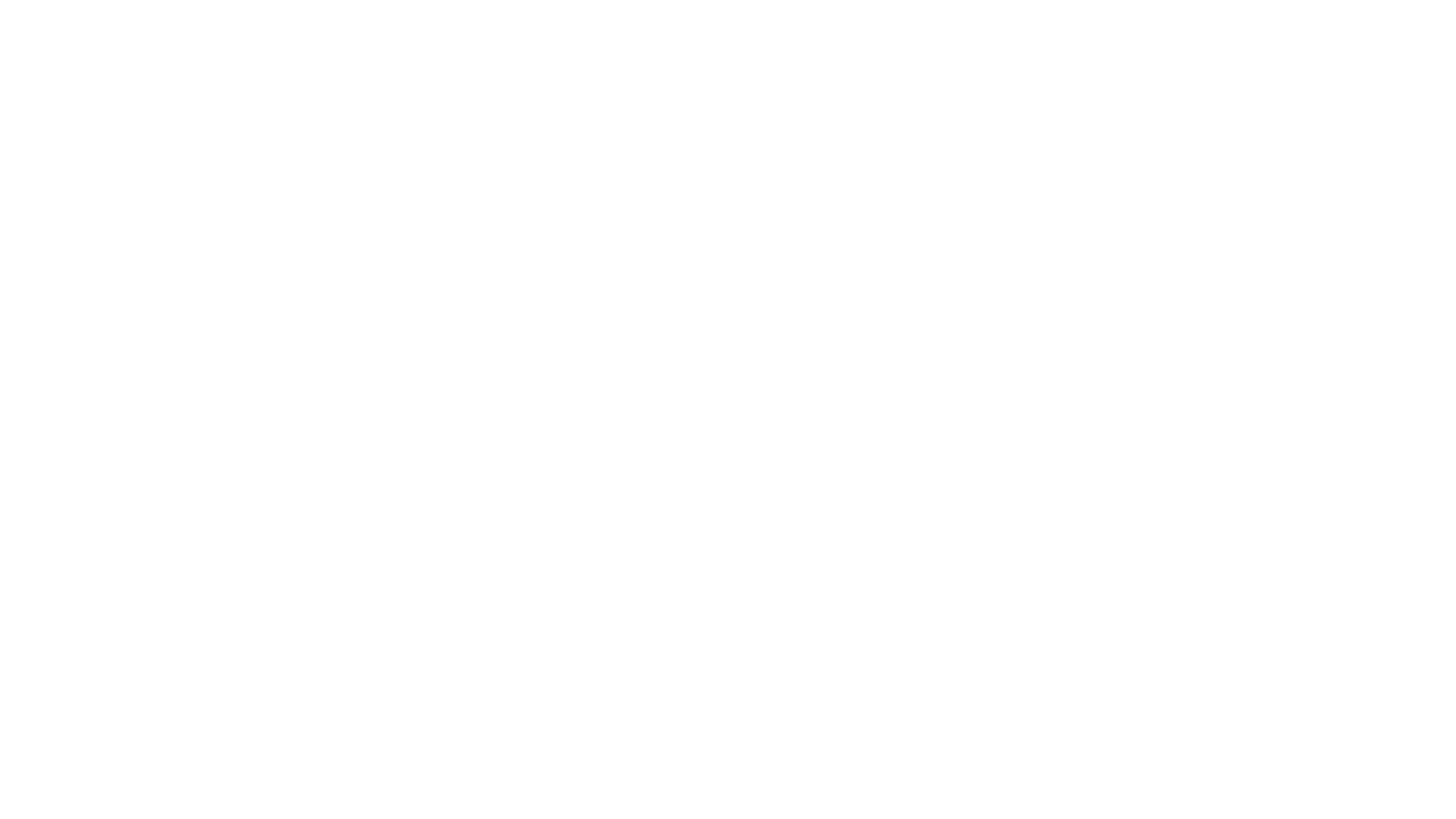-दीपक रंजन दास
घोरपडीचे शेपूट महाराष्ट्र का एक पारम्परिक खेल है। इसका शाब्दिक अर्थ है छिपकली की पूंछ। मान्यता है कि मराठा योद्धा तानाजी मालुसरे पालतू घोरपड़ का इस्तेमाल किया करते थे। घोरपड़ मानीटर लिजार्ड को कहते हैं जिसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। घोरपड़ की कमर में रस्सी बांध कर उसे किले की दीवार पर चढ़ा दिया जाता था। जब घोरपकड़ मजबूती से किले की दीवार पर चिपक जाता तो सैनिक इसी रस्सी को पकड़कर आसानी से किले के भीतर पहुंच जाते थे। इसी को आधार बनाकर इस खेल की रचना की गई है। इसी तरह आटा-पाटा, गेंदतड़ी, खो-खो जैसे उत्तरी भारत के प्रचलित देसी खेलों के साथ ही महाराष्ट्र के ‘गिधाड़ा गुढकावण’ तथा आंध्रप्रदेश के ‘नालुगु राल्लू आटा’ तथा पूर्वोत्तर की कुश्ती ‘डापो न्यारका सुनम’ को भी सातवीं कक्षा के सिलेबस में शामिल किया गया है। ‘राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद’ ने यह बदलाव नवीन शिक्षा नीति के अनुपालन में किया है। दरअसल, किसी भी खेल का विकास वहां की विरासत को प्रतिबिंबित करता है। खेल-खेल में रोचक ढंग से बच्चों को टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज के साथ ही शारीरिक दक्षता, कला कौशल एवं रणनीति बनाने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इन खेलों के माध्यम से बच्चों को फिटनेस तथा सही भोजन एवं दिनचर्या के लिए भी प्रेरित किया जा सकेगा। इन खेलों का उद्देश्य बच्चों के फिजिकल एवं मोटर फिटनेस में इजाफा करना भी है। दरअसल, अब विद्यार्थी अकादमिक स्तर पर तो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं पर जब जीवन में चुनौतियां सामने आती हैं तो वे हथियार डाल देते हैं। इन खेलों के माध्यम से बच्चे बेहतर रणनीति बनाने, चुनौतियों को अवसर में बदलने और लगातार प्रयास करते रहने के गुर सीखेंगे। इसके साथ ही अब कौशल विकास को भी सिलेबस में शामिल किया जा रहा है। इसके लिए ‘कौशल बोध’ नामक किताब लाई गई है। इसमें कठपुतली कला, टाई-डाई फैब्रिक प्रिंटिंग, बागवानी, लहरिया और बांधनी, मदुरै सुंगुड़ी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि जैसे विषयों को शामिल किया गया है। देश में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति आने के बाद पारम्परिक कौशल को बहुत नुकसान हुआ। भारतीय समाज कौशल के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण में यकीन करता था। यही इनकी जातीय पहचान भी थी। फिर नौकरियों का आकर्षण इस कदर बढ़ा कि लोगों ने अपने पारम्परिक विधा को त्याग दिया और कई प्रकार के कौशल लुप्तप्राय हो गए। आधुनिक युग में इनमें से कई कौशल नए रूप में सामने आए। नापित का पारम्परिक ज्ञान सलून के रूप में तो दर्जी का काम फैशन डिजाइनिंग के रूप में उभरा। मालागरों का काम ऑर्नामेंट डिजाइनिंग के रूप में सामने आया तो पारम्परिक नसों का ज्ञान फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टर के रूप में विकसित हुआ। जातीय बंधनों से मुक्त होकर इन विधाओं ने बेशुमार तरक्की की। अब कोशिश है कि बच्चे और उनके अभिभावक दोनों इसके मर्म को समझें। इससे पारम्परिक कौशल को आगे बढ़ाने की तकनीक भी विकसित होगी जिससे रोजगार के अवसर बनेंगे।
Gustakhi Maaf: सातवीं के बच्चे सीखेंगे ‘घोरपडीचे शेपूट’