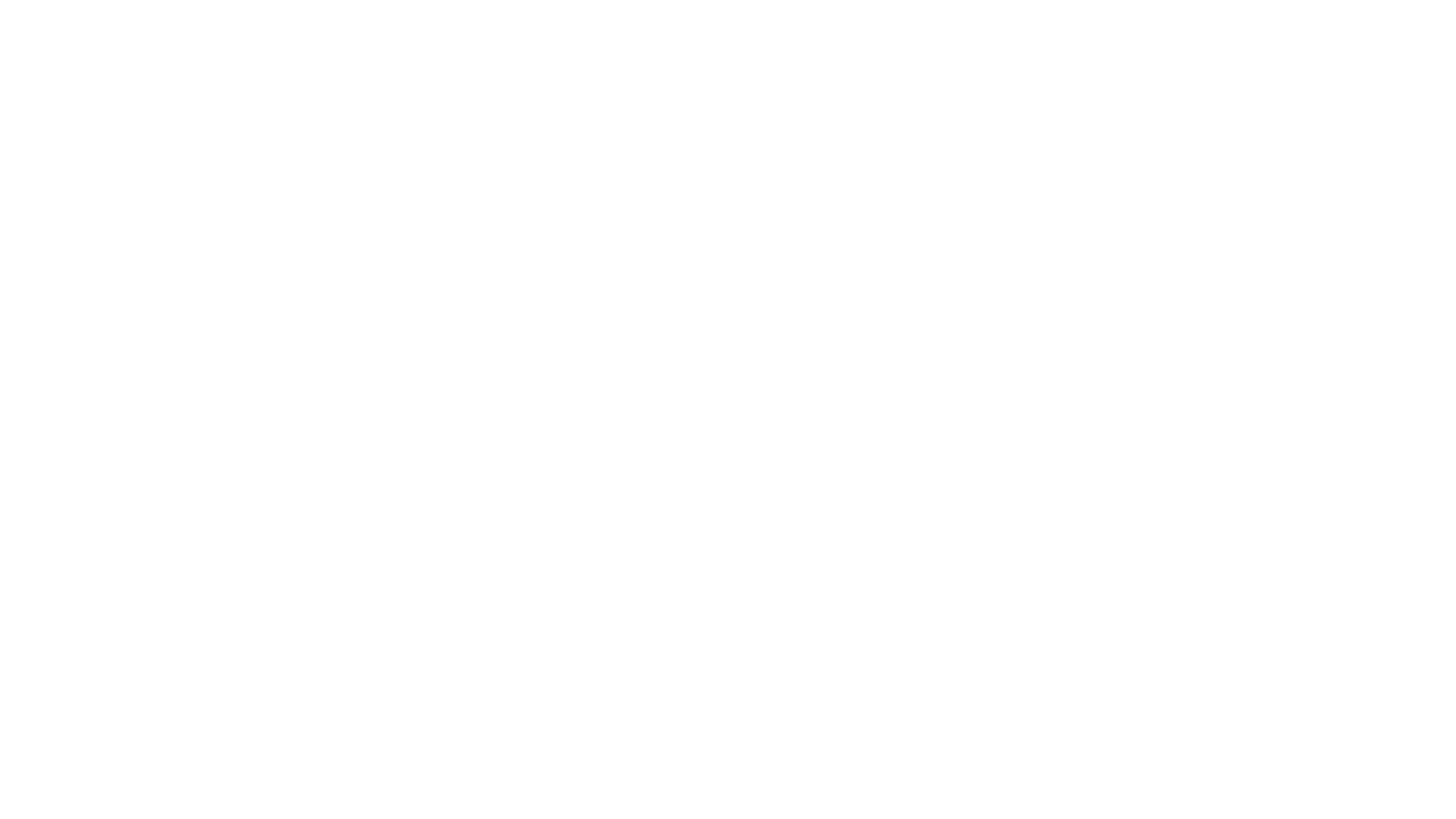-दीपक रंजन दास
सोमवार को भारत में गुरूपूर्णिमा का पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों, व्याख्याताओं और प्राध्यापकों का आशीर्वाद लिया। अधिकांश शिक्षकों ने विद्यार्थियों के सिर पर अपना हाथ रखना तक जरूरी नहीं समझा। भारतीय समाज में यह कोई रातोंरात हुआ परिवर्तन नहीं है। सृष्टि के आरंभ में ही इसकी भी नींव रखी जा चुकी थी। इस अवसर पर एक श्लोक का प्रयोग बहुतायत में किया जाता है-
गुरूब्र्रह्मा गुरूर्विष्णु: गुरूर्देवो महेश्वर:।
गुरूर्साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नम:।।
अर्थात गुरू ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। गुरू ही साक्षात् आदिब्रह्म हैं। इसी रूप में गुरू को सम्मान देते हुए उन्हें प्रणाम किया जाता है। यह मंत्र स्कंदपुराण से लिया गया है। सतयुग में यही स्थिति थी। गुरू ही सकल ज्ञान के एकमात्र स्रोत थे। युग बदलते गए और गुरू की परिभाषा और भूमिका भी बदलती गई। त्रेतायुग में गुरू ऋषि विश्वामित्र प्रभु श्रीराम को उनके पिता राजा दशरथ से मांग कर ले जाते हैं। प्रभु श्रीराम उन राक्षसों का संहार करने में सफल होते हैं जो यज्ञादि में विघ्न डाला करते थे। गुरू अपने शिष्य की क्षमताओं को जानते थे। इसी युग में मरणासन्न रावण से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर भी प्रभु श्रीराम जाया नहीं करते। द्वापर के आते-आते गुरू की स्थिति काफी बदल जाती है। श्रीकृष्ण अर्जुन के मित्र थे पर उनका स्थान गुरू का था। सम्पूर्ण महाभारत के दौरान वे अर्जुन के गुरू की भूमिका में रहे। इसी युद्ध में दुनिया को कर्मयोग का सिद्धांत देने वाले गीता का जन्म हुआ। द्वापर में हम यह भी देखते हैं कि गुरू अपने शिष्यों की जिद पूरी करने के लिए अस्त्र-शस्त्र उठाते हैं और अधर्म के पक्ष में युद्ध करने के लिए विवश हो जाते हैं। गुरू की यह बदली हुई भूमिका कौरवों के समूलनाश का कारण बनती है। अब तो कलयुग चल रहा है। न तो माता-पिता को और न ही शिक्षक को इस बात का कोई आभास है कि उनका शिष्य ज्ञान कहां से प्राप्त कर रहा है। चेला ग्राहक और गुरू व्यापारी है। बस उपभोक्ता फोरम जाना बचा है। बहरहाल, गुरूपूर्णिमा पर जिस श्लोक का इन दिनों बहुतायत में प्रयोग हो रहा है वह स्वयं भी एक अपभ्रंश है। मूल श्लोक में संस्कृत व्याकरण के नियमों के अनुसार छंदों में गुरु: और ब्रह्म, गुरु: विष्णु, का युग्म रूप प्रयोग किया जाता है। विसर्ग संधि रूप में ‘रÓ का उच्चारण प्राप्त करता है। अर्थात अलग-अलग बोलने पर गुरू: विष्णु और साथ-साथ उच्चारण करने पर गुरुर्विष्णु। पर अब एक नये शब्द का जन्म हो चुका है। गुरुर विष्णु। गुरुर कोई शब्द ही नहीं है। गुरूर फारसी शब्द है जो संभवत: मंगोल से आया है। इसका अर्थ अभिमान, अहंकार या घमण्ड है। इस शब्द का इस मंत्र में कोई स्थान नहीं हो सकता। ‘निंदक नियरे राखिए…Ó का दौर भी चला गया। गुरू हमेशा मीठा ही बोलेगा, यह जरूरी नहीं। इसलिए चमचों की चांदी है।
Gustakhi Maaf: विश्वगुरू भारत में गुरूपूर्णिमा का पर्व